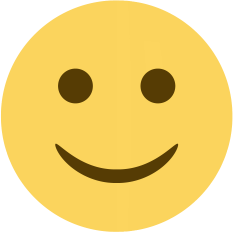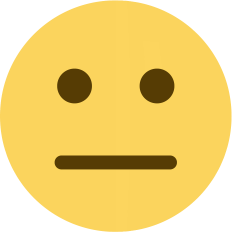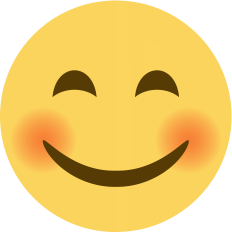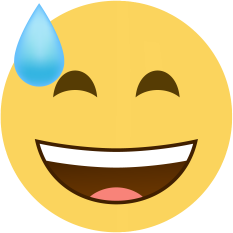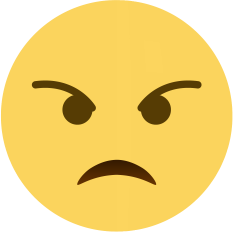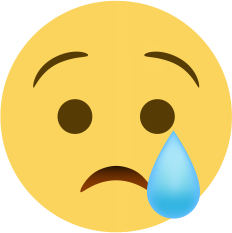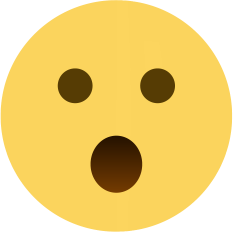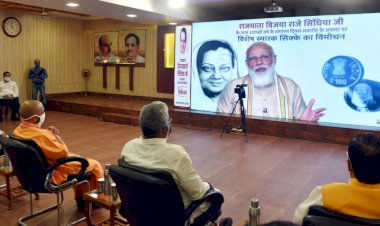आज भी प्रासंगिक है अंबेडकर के विचार

रिपोर्ट - प्रेम शंकर पाण्डेय
देश में हाल ही में डॉ भीमराव अंबेडकर की 135 वीं जयंती मनायी गयी। डॉ. अंबेडकर भारत के समाज और राजकीय व्यवस्था के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। समाज के सभी वर्ग और विशेष रूप से सभी राजनीतिक दल उनकी विरासत का दावा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस दावे की यह लड़ाई तेजी से कटु हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि अंबेडकर सभी लोगों के लिए सब कुछ हो सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अपने स्वयं के हितों के अनुरूप उनके लेखन, भाषणों और कथनों का इस्तेमाल करते हैं। अंबेडकर को समझने, उनकी व्याख्या करने या उन पर रिपोर्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके मूल लेख को उद्धृत किया जाए। अंबेडकर को पढ़ना और बार बार पढ़ना निश्चित रूप से लाभकारी है जो नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वे अपने लेखन और भाषणों में कितने दूरदर्शी थे। उदाहरण के लिए, संविधान को अपनाने से ठीक दो महीने पहले, 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के समापन सत्र में उनके सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक का जिक्र करें। उस भाषण के अंतिम भाग में वे कहते हैं-हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम पर बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी है। आजादी के बाद कुछ भी गलत होने के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना हमने खो दिया है। अगर इसके बाद चीजें गलत हो जाती हैं तो हम अपने को छोड़कर किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकेंगे। इसके बाद उन्होंने भारत के नवजात लोकतंत्र के लिए तीन जबरदस्त खतरों का उल्लेख किया। पहला है, राजनीति में नायक पूजा या व्यक्तित्व पंथ बनाने की प्रवृत्ति। उन्होंने कहा, श्भारत में भक्ति या जिसे नायक-पूजा का मार्ग कहा जा सकता है, राजनीति में एक भूमिका निभाती है जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी अन्य देश की राजनीति में नहीं होती है। धर्म में भक्ति, आत्मा के उद्धार का मार्ग हो
सकती है लेकिन राजनीति में, भक्ति या नायक-पूजा पतन और अंततरू तानाशाही के लिए एक निश्चित मार्ग है। ये शब्द आज पहले से कहीं अधिक सच हैं। यह भी विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने पंथ पूजा के खिलाफ चेतावनी दी थी, वह स्वयं पंथ पूजा की वस्तु बन गया है। वर्तमान परिदृश्य में डॉ. अंबेडकर की कोई भी आलोचना असहनीय होती जा रही है। अंबेडकर का गणतंत्र आहत भावनाओं के गणतंत्र में परिवर्तित हो रहा है जो जरा सी कथित धमकी होने पर आपराधिक मुकदमा चलाने को आमंत्रित करता है। अंबेडकर ने जिस दूसरे खतरे की ओर इशारा किया, वह यह चेतावनी थी कि संविधान में निहित राजनीतिक समानता बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानता के साथ उत्तरोत्तर असंगत होती जा रही है। उन्होंने एक सामाजिक लोकतंत्र की वकालत की थी जिसका अर्थ है जीवन का एक तरीका जो (बुनियादी) सिद्धांतों के रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मान्यता देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि खतरा यह है कि अगर बढ़ती (सामाजिक और आर्थिक) असमानता को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो वे लोग जो वचित और उत्पीड़ित थे, वे लोकतंत्र की शानदार इमारत को उड़ा देंगे जिसे उसके संस्थापकों ने इतनी मेहनत से बनाया था। उन्होंने यह चेतावनी नक्सली हिंसा की पहली घटना से लगभग 20 साल पहले दी थी। नक्सली हिंसा की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई जो हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है। हमारे चारों ओर हर जगह आर्थिक असमानता के साथ लोकतांत्रिक समानता की विसंगति के उदाहरण हैं। बढ़ते कल्याणकारी राज्य की संकल्पना और मुफ्त उपहार या सब्सिडी जो भी उन्हें कहा जाता है, अमीरों पर कर लगाकर असमानता की खाई को पाटने का एक कमजोर प्रयास है। अमेरिका में ट्रम्प का दूसरी बार राष्ट्रपति बनना लोकतांत्रिक अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था की विफलता के कारण बढ़ती आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए है। ट्रम्प का समर्थन काफी हद तक उस वर्ग से आता है जिसकी पारिवारिक आय, जीडीपी का आकार बढ़ने और शेयर बाजार की संपत्ति बढ़ने के बावजूद दशकों से स्थिर है। यूके में 2016 ब्रेक्सिट वोट भी मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा थे किया गया था जो यह महसूस करते कि वे वैश्वीकरण की ताकतों द्वारा पीछे छोड़ दिए गए हैं। अंबेडकर ने 1949 के उस भाषण में जिस तीसरे खतरे का उल्लेख किया था, वह है संवैधानिक तरीकों की पवित्रता की रक्षा करने की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके अनुसार ये कानून और व्यवस्था की अस्वीकृति के अलावा और कुछ
नहीं थे। उन्होंने मॉब लिंचिंग, सतर्कता न्याय, एनकाउंटर किलिंग और बुलडोजर न्याय जैसे संविधानेत्तर तरीके भी जोड़े होते क्योकि उनकी नजर में उनके गढ़े एक वाक्यांश के अनुसार ये विधियां और कुछ नहीं बल्कि अराजकता का व्याकरणश् हैं। यदि लोग इन तरीकों को अपनाते हैं तो यह न केवल संविधान की विफलता होगी बल्कि सत्ता की भी विफलता होगी। संविधान के क्रियान्वयन करने के लिए राज्य के अंगों-न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कार्य की आवश्यकता है। फिर भी ये अंग किस तरह से काम करते हैं यह लोगों व राजनीतिक दलों पर निर्भर करेगा। संविधान का कामकाज इसमें काम करने वाले लोगों की अच्छाई या ईमानदार इरादों पर निर्भर करता है। अंबेडकर इस बात से विशेष रूप से समझते थे कि कपटी प्रशासन के जरिए संवैधानिक प्रावधानों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। 4 नवंबर, 1948 को उन्होंने संविधान सभा में कहा था जबकि हर कोई लोकतांत्रिक संविधान के शांतिपूर्ण संचालन के लिए संवैधानिक नैतिकता के प्रसार की आवश्यकता को पहचानता है, इसके साथ दो चीजें परस्पर जुड़ी हुई हैं जो दुर्भाग्य से आम तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है।
डॉ अजीत रानाडे

 admin
admin