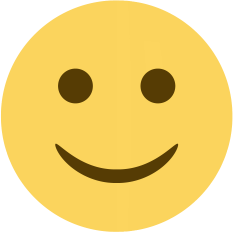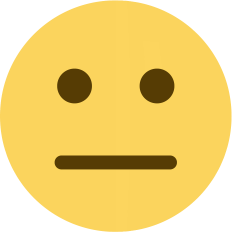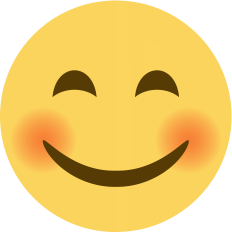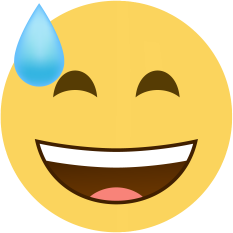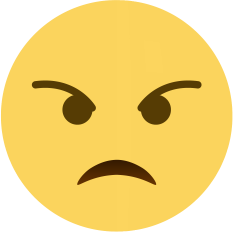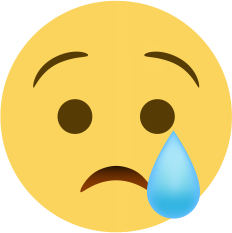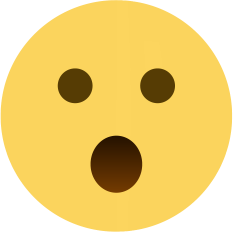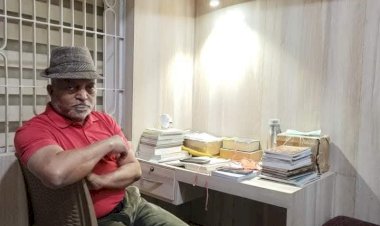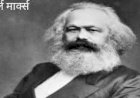प्राकृतिक संपदा के छेड़छाड़ से जलवायु के लिए बन रहा संकट

रिपोर्ट - प्रेम शंकर पाण्डेय
******************************
आज बिगड़ते पर्यावरण के चलते कई जगह'भूजल का'स्तर डेढ हजार फुट नीचे तक चला गया है।अगर हमारी उपनाऊ मिटटी इसी तरह बहती रही और जमीन बंजर होती रही,तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा?लेकिन यह काम अकेले सरकार नहीं कर सकती।इस महायज्ञ में सरकार के साथ समाज को भी खड़ा होना होगा।
हाल ही में आई धराली और उसके बाद किश्तवाड़ की आपदा वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी की भयावह यादों को जगा देती है।ये आपदाएं सख्त रूप से दोहराती हैं कि हिमालय जलवायु प्रेरित विनाश का केंद्र बनता जा रहा है।जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने और हिमनद झीलों के टूटने से बाढें आ रही हैं।ये त्रासदियां पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में आपदाओं के बढ़ते जोखिम और उनके बारे अनिश्चितता,के साथ-साथ भारत की जलवायु संबंधी बढ़ती तैयारियों में गंभीर खामियों,खासकर संवेदनशील हिमनद झीलों के व्यापक डाटाबेस के अभाव को दर्शाती हैं।ये त्रासदियां पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में अनियोजित और अनियमित विकास के परिणामों को भी उजागर करती हैं।बीते दो दश्कों में हिमालयी क्षेत्र में तीव्र गति से हुए सड़क,होटल और जलविद्युत परियोजनाओं जैसे निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय आकलन का अभाव देखा गया है।बस्तियां उन क्षेत्रों में फैल गई,जिन्हें कभी सुरक्षित मानते थे लेकिन जलवायु परिवर्तन ने नियम पलट दिए हैं।बर्फ के पिघलने से बनीं हिमनद झीलें अब टाइम बम बन गई हैं तथा निगरानी तंत्र और पूर्ण चेतावनी प्रणालियों की कमी निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों को असुरक्षित बना रही है।
केदारनाथ,सिक्किम,हिमाचल प्रदेश और अब धराली व किश्तवाड़ से पर्यावरण जो संकेत देना चाहता है,वे स्पष्ट हैं।अक्सर देखा जाता है कि आपदा के बाद राहत-बचाव कार्य को लेकर तेजी दिखाई जाती है,लेकिन इस बात के प्रयास नहीं किए जाते कि इन आपदाओं से बचा जा सके।ये आपदाएं न सिर्फ बड़े स्तर पर जीवन व आजीविका को क्षति पहंचाती हैं बल्कि वे बुनियादी ढांचे पर चोट कर आवागमन व कच्चे माल की उपलब्धता को बाधित करके आपूर्ति श्रृखलाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं।जलवायु परिवर्तन की वजह से आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले व्यवधानों और बुनियादी ढांचे को होनें वाले नुकसान के खिलाफ भारत का संघर्ष तेज होता जा रहा है,जिससे कठिन चुनौतियां भी सामने आ रही है।
ओडिशा के बाढ़ संभावित जिले जगतसिंहपुर की जिला आपदा प्रबंधन योजना 2025 में कमजोरियों को रेखांकित करते हुए बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ ही जल निकासी में सुधार और आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्रों के निर्माण की सिफारिश की गई है।तमिलनाडु के अंबतूर औद्योगिक क्षेत्र ने चक्रवातों के दौरान बाढ़ के मार्गों को बहाल करने और जल भराव को रोकने के लिए 50 करोड़ रुपये की एक पहल शुरू की है।महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के जोखमों का समाधान ढलान स्थिरीकरण, पुनर्वनीकरण और आपदा मानचित्रण के माध्यम से किया जा रहा है-जिसमें इंजीनियरिंग और सामुदायिक,दोनों की सहभागिता है।फिर भी,ये पहलें एक खंडित राष्ट्रीय तस्वीर को दर्शाती हैं।भारत का ज्यादातर औद्योगिक बुनियादी ढांचा बढ़ती जलवायु अस्थिरता से निपटने लिए अब भी अपर्याप्त है।
हालांकि,भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी की ओर से जलवायु जोखिम से निपटने को लेकर आदेश दिए हैं, लेकिन कड़ाई से पालन के बिना इनके कागजी कार्यवाई बनकर रह जाने की आशंका है।इस मामले में वियतनाम से कुछ सबक ले सकते है।वहां तूफान प्रभावित आत्यंतिक केंद्रों में केंद्रीकृत आमादा तैयारी योजनाओं में व्यापक जोखिम आंकलन,खाद मानचित्रण और त्वरित परिसंपत्ति सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल होते हुए ह्यू सिटी का विस्तृत बाद मानचित्रण इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे डाटा आधारित शहरी और आपूर्ति श्रृखला नियोजन जलवायु तैयारी को बेहतर बना सकता है।इसके विपरीत भारत को प्रतिक्रियाशील बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर निर्भरता छिटपुट और स्थान विशिष्ट तक सीमित होती है,जिसमें दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए आवश्यक सामंजस्य का अभाव होता है।भारत की जलवायु रणनीति को पैचवर्क परियोजनाओं से आगे बढ़कर प्रणालीगत सुधार करने होंगे, जिसके लिए एआई समेत तमाम तकनीकें सहायक हो सकती है।विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में जहां जलवायु परिवर्तन नदी मार्गो,घाटी संरचनाओं और हिमनद स्थिरता को तेजी से बदल रहा है।
धराली और किश्तवाड की आपदाएं स्थानीय न होकर, राष्ट्रीय चेतावनियां हैं।इसके लिए हिमालयी राज्यों में हिमनद झीलों की निगरानी, जोखिमों का आकलन और जलवायु-प्रतिरोधी बस्तियों की योजना बनाने हेतु एक समन्वित रणनीति की आवश्यकता है।इन क्षेत्रों को न केवल आपदा राहत में,बल्कि दीर्घकालिक वैज्ञानिक अध्ययनों,रियल टाइम निगरानी प्रणालियों और सामुदायिक तैयारियों में भी सहायता की आवश्यकता है।यह कॉर्पोरेट छवि या सरकारी वादों के बारे में नहीं है।यह वास्तविकता का सामना करने और ऐसे मजबूत बुनियादी ढांचे भौतिक,डिजिटल, नियामक और सामाजिक निर्माण के बारे में है,जो जलवायु परिवर्तन की वजह से आज और कल आने वाले तूफानों का सामना करने के लिए भी बेहद जरूरी है।
( लेखक:-रामाश्रय यादव जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद मऊ व सामाजिक चिंतक है। मोबाईल.....9415276144)

 admin
admin