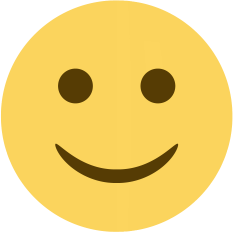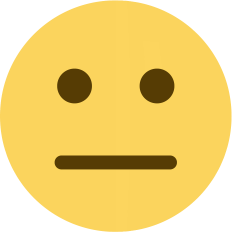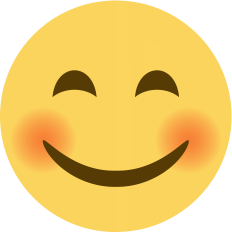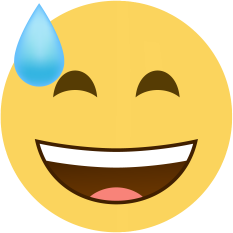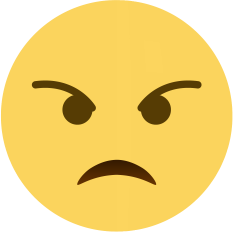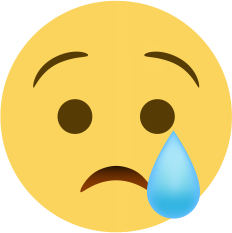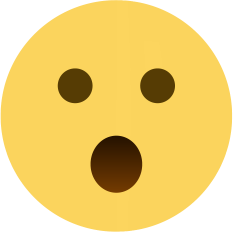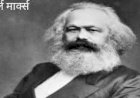बच्चों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक - डा. मनोज तिवारी

रिपोर्ट - प्रेम शंकर पाण्डेय
स्कूली बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आवश्यक
स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि 5 में से 1 बच्चे में निदान योग्य भावनात्मक, व्यवहारिक या मानसिक स्वास्थ्य विकार है और 10 में से 1 युवा में मानसिक स्वास्थ्य चुनौती पायी जाती हैं। 10-15 वर्ष के 10 में से 1 से अधिक बच्चों का कहना है कि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है या अगर वे चिंतित या उदास महसूस करते हैं तो स्कूल में किसी से बात नहीं कर पाते हैं। शोध से पता चलता है कि 50% मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं 14 वर्ष की आयु तक तथा 75% मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं 24 वर्ष की आयु तक शुरू हो जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में 23% स्कूली बच्चे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं जिनमें से अधिकांश बच्चों को मानसिक विकारों के लिए उचित इलाज नहीं मिल पाता।
स्कूली शिक्षा का उम्र 6 से 14 वर्ष होता है, जो विकास के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, साम्वेगिक, संज्ञानात्मक व शैक्षिक विकास तेजी से होता है। इस उम्र के विकास में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यदि बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता तो उसका अन्य क्षेत्रों का विकास भी सही गति, समय और मात्रा में नहीं होता है क्योंकि विकास के सभी आयाम (शारीरिक, मानसिक, साम्वेगिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यवसायिक, पारिवारिक, आर्थिक, भाषा, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं अन्य) एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक आयाम का विकास अच्छा होगा तो यह अन्य आयामों के विकास को बढ़ावा देता है और यदि एक आयाम का विकास किसी भी कारण से बाधित होता है तो यह अन्य आयामों के विकास में भी रुकावट डालता है। इसे एक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है जैसे- एक बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं होने पर वह शारीरिक रूप से कमजोर होगा और वह हमउम्र बच्चों के साथ खेलने नहीं जाता है या कम जाता है या जाने पर हार जाता है या और बच्चों से पीछे रह जाता है तो वह हमउम्र बच्चों के बीच जाना बंद कर देता है, इससे उसका भाषा विकास ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि भाषा एक अर्जित गुण है जिसमें हमउम्र लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह हमेशा पीछे रह जाने/हार जाने के कारण दुखी होगा, उसका आत्मविश्वास निम्न स्तर का होगा अर्थात उसका साम्वेगिक विकास अच्छा नहीं होगा। ऐसे बच्चे स्कूल में अनुपस्थित अधिक होते हैं और जब स्कूल जाते भी हैं तो नकारात्मक संवेग के कारण वे ठीक से सीखने में सक्षम नहीं होते। शिक्षा का संचालन भाषा में होता है और इन बच्चों का भाषा विकास निम्न स्तर का होने के कारण तथ्यों को इन्हें समझने में कठिनाई होती है, इसलिए उनका शैक्षिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है, शैक्षिक विकास ठीक से ना होने से व्यक्ति को अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती या अच्छा व्यवसाय भी स्थापित करने में कठिनाई होती है। अच्छी शिक्षा व व्यवसाय न होने पर उसके उसे अच्छे जीवनसाथी मिलने की संभावना कम होती है जिससे उसका पारिवारिक विकास भी ठीक से नहीं होता। अच्छी नौकरी या व्यवसाय न होने से व्यक्ति का आर्थिक विकास अच्छा नहीं होता तथा व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों में भी सहभागिता ठीक से नहीं कर पाता जिससे उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है।
स्कूल जाने की उम्र में बच्चे शारीरिक समस्याओं को अभिव्यक्त करने में तो सक्षम होते हैं किंतु अपने मानसिक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने व उसे दूसरों को समझाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस उम्र के बच्चों में चिंता, उदासी, निराशा, कुंठा, अलग होने का भय, असफल होने का अत्यधिक भय, परीक्षा का अधिक तनाव, दूसरों से प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा, परीक्षा में असफल होने की दुश्चिंता, सोशल मीडिया के प्रति अत्यधिक लगाव, इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं (स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविजन......) की अधिक चाहत जैसे व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक समस्याएं देखने को मिलती हैं।
एक छात्र का केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ रहना ही आवश्यक नहीं है अपितु उसे साम्वेगिक रूप से भी स्वस्थ होना उसके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है एक छात्र में अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, लोगों के साथ तार्किक संबंध स्थापित करने की क्षमता तथा उम्र एवं वरिष्ठता के अनुसार लोगों के साथ अंतः क्रिया करने की योग्यता का विकास होना आवश्यक है। छात्रों को अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीखना अत्यंत आवश्यक है, तभी वे अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने में सक्षम होंगे उन्हें दूसरों के संवेदनाओं के प्रति उचित ढंग से प्रतिक्रिया करना भी सीखना आवश्यक होता है।
विद्यालय जाने वाली उम्र में बच्चों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना शारीरिक रूप से स्वस्थ होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने में सक्षम होंगे, दिन प्रतिदिन के तनाव का सामना करने में सक्षम होंगे, नई एवं विषम परिस्थितियों में प्रभावी समायोजन करने में सफल होंगे तथा समाज में अपनी सही योगदान कर सकेंगे। एक मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र के लक्षण :-
1- विवेकशील चिंतन की क्षमता
2- समस्या समाधान की क्षमता
3- सृजनात्मक कौशल
4- नए एवं उपयोगी संप्रत्यय को सीखने में सफल होंगे।
5- शिक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होंगे।
6- नई एवं विषम स्थितियों में भी प्रभावशाली समायोजन
7- धनात्मक संवेगों को बनाए रखने की क्षमता
8- नकारात्मक संवेगों पर नियंत्रण रखने में सफल होंगे
*मानसिक स्वास्थ का शिक्षा पर प्रभाव:*
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का उनके शैक्षिक विकास पर सीधा एवं गंभीर प्रभाव पड़ता है। शोधों में यह स्पष्ट हुआ है कि मानसिक समस्याओं से ग्रस्त बच्चे सीखने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हैं। मानसिक समस्याओं के पीछे नकारात्मक संवेगों- भय, क्रोध, घृणा, आत्मविश्वास में कमी, असहाय महसूस करना, विश्वास की कमी इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह सर्वविदित है कि जब बच्चे नकारात्मक संवेग में होते हैं तो वे अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे- अधिगम, स्मृति, चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता और प्रत्यक्षीकरण आदि का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो अपने पर नियंत्रण खो देता है और अपना या अपनों का ही हानि कर देता है । भय में विस्मरण की गति तीव्र हो जाती है।
*शिक्षा का मानसिक स्वास्थ पर प्रभाव*: शिक्षा की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्कूल के वातावरण, अनुशासन, शिक्षकों का छात्रों के प्रति व्यवहार, शिक्षकों का व्यक्तित्व, सहपाठियों का आपस में संबंध, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ के साथ छात्रों का आपस में व्यवहार, शिक्षक की शिक्षण शैली, शिक्षक की भाषा शैली एवं विद्यालय कर्मियों का व्यवहार भी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विद्यालय में निम्नलिखित प्रयास किए जाने आवश्यक है :
1- स्कूल का वातावरण- भौतिक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक सहयोगात्मक एवं सौहार्दपूर्ण होना चाहिए।
2- शिक्षण योजना का निर्माण छात्रों के रूचि, योग्यता एवं आवश्यकता के अनुरूप करना चाहिए।
3- शिक्षण विधि का चुनाव छात्रों के उम्र, परिपक्वता एवं विषयवस्तु के अनुरूप करना चाहिए।
4- पाठ्यक्रम का चुनाव करते समय छात्रों की योग्यता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
5- स्कूल में मनोरंजन की संतुलित एवं समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जैसे- खेलकूद, गायन-वादन, नृत्य, संगीत, बागवानी, श्रमदान, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड का भी समय-समय पर आयोजन किया जाना चाहिए।
7- शिक्षकों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण, सहयोगात्मक एवं आदर्श होना चाहिए।
8- शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधन को छात्रों की समस्या को ध्यान से सुनना एवं सहानुभूतिपूर्वक समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।
9- छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए इसके लिए उन्हें उनके योग्यता के अनुरूप चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने का अवसर देना चाहिए जब वे ऐसे कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा वे अपने जीवन के कठिन एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का भी सामना करने में स्वयं से सक्षम होंगे।
10- शिक्षकों को छात्रों की सभी समस्याओं को हल नहीं करना चाहिए अपितु उन्हें समस्या हल की प्रक्रिया को सीखने में सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि भविष्य में वे अपनी समस्याओं का स्वयं से समाधान करने में सक्षम हो सके।
11- विद्यालयों का अनुशासन संतुलित एवं तर्कसंगत होना चाहिए, बहुत सख्त अनुशासन छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती है।
12- शिक्षकों को सभी छात्रों से एक समान अपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर छात्र एक दूसरे से भिन्न होता है उनकी क्षमताएं अलग अलग होती है, अनावश्यक रूप से दूसरों से तुलना उनके लिए मानसिक समस्या उत्पन्न कर सकता है।
13- पुनर्बलन एवं अभिप्रेरणा का उपयोग समुचित रूप से बिना भेदभाव के करना चाहिए
14- स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए तथा बच्चों में सहयोग की भावना के विकास के लिए भी पर्याप्त प्रयास करते रहना चाहिए।
15- छात्रों को शुरू से ही परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए उन्हें परीक्षा को एक अवसर के रूप में लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए न कि बाधा के रूप में ।
16- दण्ड का उपयोग करने से यथासंभव बचना चाहिए अपेक्षित व्यवहारों को बढ़ाने तथा अनपेक्षित व्यवहारों में कमी लाने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग आसानी से किया जा सकता है।
*बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में माता-पिता की भूमिका:*
बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में उनके माता-पिता की अहम् भूमिका होती है। घर का वातावरण, माता-पिता का आपस में संबंध तथा उनका बच्चों के प्रति व्यवहार, परिवार के सदस्यों का बच्चों के प्रति व्यवहार, भाई बहनों का आपस में संबंध, मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता, आस-पड़ोस का वातावरण, बच्चों के व्यवहार व मानसिक स्वास्थ्य को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। अभिभावकों को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए निम्न उपाय करने चाहिए :
1- तार्किक अनुशासन रखना चाहिए।
2- बच्चों की आवश्यकताओं की संतुष्टि समुचित रूप से करना चाहिए।
3- बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करना चाहिए।
4- बच्चों से उनकी योग्यता/क्षमता से अधिक अपेक्षा नहीं करना चाहिए
5- बच्चों को उनके क्षमता के अनुरूप कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए
6- बच्चों को उनके अच्छे कार्यों एवं प्रयासों के लिए शाबाशी, पुनर्बलन व पुरस्कार देना चाहिए।
7- बच्चों की तुलना अतार्किक रूप से दूसरे बच्चे से नहीं करना चाहिए।
8- अपने इच्छाओं एवं अपने अपूर्ण लक्ष्यों को बच्चों को ऊपर नहीं थोपना चाहिए।
9- आवश्यक होने पर बच्चों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए किंतु उनके इंटरनेट उपयोग के समय को निर्धारित करना चाहिए तथा बीच-बीच में उनके द्वारा इंटरनेट पर किए जा रहे कार्यों का अवलोकन करते रहना चाहिये।
बच्चों का मन कोमल एवं मस्तिष्क विकासशील होता है उनके प्रति किया गया असंगत व कठोर व्यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती का कार्य करता है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसमें माता-पिता, भाई- बहन, परिवार के सदस्यों, साथी समूह, शिक्षक एवं विद्यालय कर्मियों के साथ-साथ समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब सभी लोगों के द्वारा व सभी जगहों पर बच्चों के साथ समुचित व्यवहार किया जाएगा तभी बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम होगा और वह अपनी पूरी क्षमता से समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम होंगे। जैसा कहा गया है कि *बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं* इस दृष्टिकोण से भी बच्चों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

साभार
डा.मनोज कुमार तिवारी ✍️
वरिष्ठ परामर्शदाता
एआरटीसी, एस एस हॉस्पिटल, आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी

 admin
admin